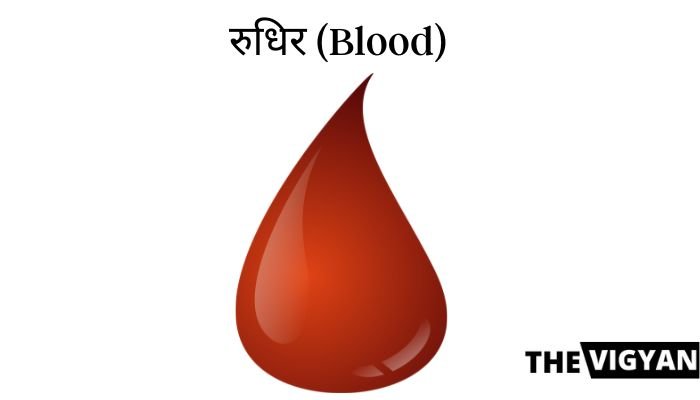इस आर्टिकल में हम रुधिर (Blood) जिसे खून या ब्लड भी कहा जाता है के बारे में बतायेगे | इस आर्टिकल में हम जानेगे कि रुधिर क्या होता है ? रुधिर का शरीर के लिए क्या महत्त्व है ? रुधिर के कार्य क्या है ? रुधिर के प्रमुख घटक कोनसे है ? रुधिर कोशिकाय क्या है ? लाल रुधिर कोशिकाएँ, श्वेत रुधिर कोशिकाएँ, विंबाणु, या प्लेटलेट् क्या होते है ? प्लाज्मा (Plasma) क्या होता है ? हीमोग्लोबिन (Haemoglobin) क्या होता है ? खून का स्कन्दनयाथक्का कैसे जमता है ? Rh-समूह और रुधिर समूह (Blood Group) क्या होते है ? लसिका क्या है ? आदि |
रुधिर क्या होता है ? (What is Blood)
रुधिर एक लाल, वाहक संयोजी ऊतक (vascular connective tissue) है, जो एक चिपचिपा अपारदर्शी द्रव है। इसकी श्यानता (viscosity) 4.7 तथा क्षारीय प्रकृति (pH 7.54) होती है। ऑक्सीकृत रुधिर चमकीले लाल रंग का होता है, जबकि अनॉक्सीकृत रुधिर गुलाबी नीले रंग का होता है। रूधिर में प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाएँ होती है |
यह सम्पूर्ण शरीर का लगभग 6-10% भाग बनाता है। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5.8 लीटर रुधिर पाया जाता है। ऊँचे स्थानों पर रहने वाले लोगों में नीचे स्थानों पर रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक रुधिर पाया जाता है। रुधिर दो भागों यथा प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं का बना होता है।
उच्च अकशेरुकी , कशेरुकी एवं मानव में पोषक पदार्थो , गैसों , हार्मोन , अपशिष्ट पदार्थों एवं अन्य उत्पादों के परिवहन के लिए रुधिर पाया जाता है जिसे एक पेशीय ह्रदय द्वारा पम्प किया जाता है , इस सम्पूर्ण तंत्र को परिसंचरण तन्त्र कहते है , परिसंचरण तंत्र के निम्न भाग होते है –
(i) रुधिर (ii) ह्रदय (iii) रुधिर वाहिकाएँ (iv) रुधिर (blood)
रुधिर के दो भाग है : (1) द्रव भाग, जिसे प्लाज़्मा कहते हैं और (2) ठोस भाग, जो कोशिकाओं का बना होता है। रुधिर कोशिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं : (1) लाल रुधिर कोशिकाएँ (2) श्वेत रुधिर कोशिकाएँ और (3) विंबाणु, या प्लेटलेट्। प्लाज़्मा में 91 से 92 प्रति शत जल और शेष में (क) सोडियम, पोटैशियम और कैल्सियम, (ख) वसा, (ग) शर्करा, (घ) प्रोटीन आदि होते हैं।

प्लाज्मा (Plasma)
प्लाज्मा पीले रंग का निर्जीव द्रव है, जो हल्का क्षारीय होता है। यह रुधिर के सम्पूर्ण आयतन का लगभग 55-60% भाग होता है।
प्लाज्मा के संघटक
जल – 90-62%
अकार्बनिक लवण – 1-2%
प्लाज्मा प्रोटीन – 6-7%
अन्य अकार्बनिक यौगिक – 1-2%
| अवयव | मात्रा | प्रमुख कार्य |
| 1. जल | 90% | रुधिर दाब व आयतन बनाए रखना |
| 2. कार्बनिक पदार्थ | ||
| (a) एल्बुमिन | 45% | परासरण दाब उत्पन्न करना |
| (b) ग्लोबुलिन | 2.5% | परिवहन व प्रतिरक्षी उत्पन्न करना |
| (c) फाइब्रिनोजन | 0.3% | रुधिर स्कंदन |
| (d) प्रोयोम्बिन | – | रुधिर स्कंदन |
| (e) ग्लूकोज | 0.1% | पोषक पदार्थ , कोशिकीय इंधन |
| (f) एमीनो अम्ल | 0.4% | पोषक पदार्थ |
| (g) वसा अम्ल | 0.5% | पोषक पदार्थ |
| (h) हार्मोन एंजाइम | – | नियामक पदार्थ |
| (i) यूरिया , यूरिक अम्ल | 0.4% | अपशिष्ट पदार्थ |
| (j) अकार्बनिक पदार्थ | 0.9% | विलेय विभव एवं pH का नियमन करना |
प्लाज्मा के कार्य (Function of Plasma)
सरल भोज्य पदार्थों (ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि) का आँत्र एवं यकृत से शरीर के अन्य भागों से में परिवहन करता है।
यह उपापचयी वर्ज्य पदार्थों; जैसे- यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का ऊतकों से वृक्कों (kidney) तक उत्सर्जन हेतु परिवहन करता है।
यह अन्तःस्रावी ग्रन्थि से लक्ष्य अंगों तक हॉर्मोनों का परिवहन करता है।
यह रुधिर का pH स्थिर रखने में सहायक होता है।
प्लाज्मा में उपस्थित रुधिर प्रोटीन एवं फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं ।
रुधिर कणिकाए (Blood Corpuscles or Blood Cells)
ये कोशिकाएँ प्लाज्मा में पाई जाती हैं, जो रुधिर प्लाज्मा का 40-45% भाग होती है। रुधिर कणिकाओं का प्रतिशत हीमेटोक्रिट मूल्य (Haematocrit Value) या पैक्ड सैल वॉल्यूम) (Packed Cell Volume) कहलाता है। इसमें तीन कणिकाएँ – लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ तथा रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं।
लाल रुधिर कणिकाएँ (Red Blood Corpuscles-RBCs)
ये स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकियों में अण्डाकार, द्विउत्तल एवं केन्द्रकीय होती हैं। स्तनियों में (ऊँट एवं लामास को छोड़कर) RBCs गोलाकार, द्विअवतल और केन्द्रक विहीन होती हैं। लाल रुधिर कोशिकाएँ लाल रंग की होती हैं। हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग लाल होता है। ये 7.2 म्यू व्यास की गोल परिधि की और दोनों ओर से पैसे या रुपए के समान चिपटी होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता। वयस्क पुरुषों के रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर में लगभग 50 लाख और स्त्रियों के रुधिर के प्रति घन मिलिमीटर में 45 लाख लाल रुधिर कोशिकाएँ होती हैं। इनकी कमी से रक्तक्षीणता तथा रक्त श्वेताणुमयता (Leukaemia) रोग होते हैं। इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते है |
RBCs की अतिरिक्त मात्रा प्लीहा (spleen) में संग्रहित होती है, जो रुधिर बैंक (Blood Bank) की भाँति कार्य करती है। गर्भस्थ शिशु में RBCs का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में, जबकि शिशु के जन्म के उपरान्त इसका निर्माण मुख्यतया अस्थि मज्जा (bone-marrow) में होता है। मनुष्य का RBCs का औसत जीवनकाल 120 दिन का, जबकि मेंढक एवं खरगोश के RBCs का औसत जीवनकाल क्रमशः 100 तथा 50-70 दिन होता है।
लाल रुधिर कोशिका का विकास
आधुनिक मत के अनुसार लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण रक्त परिसंचरण तंत्र के बाहर होता है।सबसे पहले बनी कोशिका हीमोसाइटोब्लास्ट (Haemoctoblast) कहलाती है। पीछे यह कोशिका लाल रुधिर कोशिका में बदल जाती है। भ्रूण में लाल रुधिर कोशिका रुधिर परिसंचरण क्षेत्र में बनती है। पहले इसके मध्य में केंद्रक होता है, जो पीछे विलीन हो जाता है। शिशुओं के मध्यभ्रूण जीवन से लेकर जन्म के एक मास पूर्व तक लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। शिशु जन्म के बाद लाल रुधिर कोशिकाएँ अस्थिमज्जा में बनती हैं।
हीमोग्लोबिन (Haemoglobin)

RBCs में एक लाल प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो एक प्रोटीन ग्लोबिन (96%) तथा रंजक हीम (4-5%) से बना होता है। हीम अणु के केन्द्र में ‘लौह’ होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है । RBCs का रंग वैसे तो पीला होता है, परन्तु हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है।
हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और इसको रक्त द्वारा सारे शरीर में पहुँचता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.5 ग्राम प्रतिशत है। अनेक रोगों में इसकी मात्रा कम हो जाती है। हीम (Haem) का सूत्र (C34 H30 N4 O4 FcOH) है। इसमें लोहा रहता है। इसमें चार पिरोल समूह रहते हैं, जो क्लोरोफिल से समानता रखते हैं। इसका अपचयन और उपचयन सरलता से हो जाता है। अल्प मात्रा में यह सब प्राणियों और पादपों में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्रिस्टलीय रूप से सरलता से प्राप्त हो सकता है।
रुधिर परीक्षा के लिए वयस्क व्यक्ति की अंगुली से या शिरा से रुधिर निकाला जाता है। रुधिर को जमने से बचाने के लिए स्कंदन प्रतिरोधी पदार्थ डालते हैं। इसके लिए प्राय: अमोनियम और पोटैशियम ऑक्सेलेट प्रयुक्त किए जाते हैं।
डबल ऑक्सेलेटेड रुधिर को लेकर, अपकेंद्रित में रखकर, आधे घंटे तक घुमाते हैं। रुधिर का कोशिकायुक्त अंश तल में बैठ जाता है और तरल अंश ऊपर रहता है। यही तरल अंश प्लैज़्मा है।
RBCs की संख्या का निर्धारण हीमोसाइटोमीटर द्वारा किया जाता है। इसकी संख्या WBCs (White Blood Corpuscles) से अधिक होती है।
हेमरेज (Haemorrhage) एवं होमोलाइसिस (Haemolysis) से RBCs की संख्या घट जाती है, जिसे एनिमिया (Anaemia) कहा जाता है। RBCs की संख्या में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि पॉलीसाइमिया (polycythemia) कहलाती है।
श्वेत रुधिर कणिकाएँ (White Blood Corpuscles-WBCs)
इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते है | ये आकार में गोल अथवा अमीबाकार, केन्द्रकयुक्त तथा वर्णकविहीन कणिकाएँ होती हैं। WBCs का आकार RBCs से बड़ा, जबकि संख्या में RBCs से कम होती है। ल्यूकीमिया (रुधिर कैंसर) में WBCs की संख्या बढ़ जाती है। इनका निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा में होता है , इनमें हिमोग्लोबिन का अभाव होता है परन्तु केन्द्रक उपस्थित होता है , इनकी संख्या 6000 -8000 प्रतिघन मि.मी होती है | WBC की औसत आयु 45 दिन की होती है | ये लाल रुधिर कोशिकाओं से पूर्णतया भिन्न होती हैं। कुछ श्वेत रुधिर कोशिकाओं में कणिकाएँ होती हैं।
श्वेत रुधिर कोशिकाओं में जीवाणुओं के भक्षण करने की शक्ति होती है। संक्रामक रोगों के हो जाने पर इनकी संख्या बढ़ जाती है, पर मियादी बुखार, या तपेदिक हो जाने पर इनकी संख्या घट जाती है। श्वेत रुधिर कोशिकाएँ दो प्रकार की होती हैं, एक में कणिकाएँ नहीं होतीं और दूसरी में कणिकाएँ होती हैं। पहले प्रकार को एग्रैन्यूलोसाइट्स (Agranulocytes) और दूसरे प्रकार को ग्रैन्यूलोसाइट्स (Granulocytes) कहते हैं।
एग्रैन्यूलोसाइट्स कोशिकाएँ दो प्रकार की होती हैं : (1) लसीकाणु (Lymphocyte) कोशिका और (2) मोनोसाइट (Monocyte) कोशिका। लसीका कोशिकाएँ लघु और विशाल दो प्रकार की होती है। मोनोसाइट कुल श्वेत रुधिर कोशिकाओं की 5 से 10 प्रतिशत तक होती हैं।
ग्रैन्यूलोसाइट कोशिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं : (1) न्यूट्रोफिल्स (Neutrophiles, 60 से 70 प्रतिशत), (2) ईओसिनोफिल्स (Eosinophilesm, 1 से 4 प्रतिशत) और (3) बेसोफ़िल्स (Basophiles 0.5 से 1 प्रतिशत)।
ग्रेन्यूलोसाइट्स (Granulocytes)
ये कोशिकाएँ लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं।
ये कुल ल्यूकोसाइट्स की लगभग 65% होती हैं।
ये केन्द्रक के आकार एवं उनके कणों की अभिरंजक क्रियाओं के आधार पर पुनः निम्न प्रकार विभाजित की जा सकती हैं :
न्यूट्रोफिल्स (Neutrophils)
ये WBCs की कुल संख्या का लगभग 62% होती है।
इनके कोशिकाद्रव्य में महीन कण पाए जाते हैं, जो अम्लीय एवं क्षारीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होते हैं तथा बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं।
ये शरीर के रक्षक की भाँति कार्य करती हैं
न्यूट्रोफिल्स शरीर की रक्षा, एसिडोफिल्स घावों को भरने, बेसोफिल्स रुधिर का थक्का जमाने, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षियों का संश्लेषण तथा मोनोसाइट जीवाणुओं का भक्षण का कार्य करती है।
बेसोफिल्स (Basophils)
ये सायनोफिल्स भी कहलाती हैं।
कोशिकाद्रव्यी कण बड़े होते हैं, जो नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं।
ये हिपेरिन एवं हिस्टेमिइन (histamine) को स्रावित कर कोशिकाओं में रुधिर का थक्का जमने से रोकती हैं।
एसिडोफिल्स (Acidophils)
इनका केन्द्रक द्विपालीयुक्त (bilobed) होता है।
एलर्जी में इनकी संख्या बढ़ जाती हैं।
ये घावों को भरने में सहायक होती हैं।
एग्रेन्यूलोसाइट्स (Agranulocytes)
ये कुल WBCs का लगभग 35% भाग होती है।
एग्रेन्यूलोसाइट्स को मोनोसाइट्स (Monocytes) व लिम्फोसाइट्स में विभाजित किया जा सकता है
मोनोसाइट्स (Monocytes)
ये सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट्स (WBCs) है।
इनका केन्द्रक अण्डाकार, वृक्क अथवा घोड़े की नाल के आकार का और बाह्य केन्द्रीय होता है।
इनका निर्माण लिम्फनोड एवं प्लीहा में होता है।
ये अत्यधिक चल होती हैं तथा जीवाणु एवं अन्य रोगकारक जीवों का भक्षण करने का कार्य करती हैं।
लिम्फोसाइट्स (Lymphocytes)
ये ल्यूकोसाइट्स (WBCs) का लगभग 30% भाग बनाती हैं।
इनका केन्द्रक बड़ा और गोल होता है तथा कोशिकाद्रव्य पतली परिधीय परत बनाता है।
ये प्रतिरक्षियों का निर्माण कर शरीर के प्रतिरक्षा तन्त्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।
श्वेत रुधिर कोशिकाएँ निम्नलिखित कार्य करती हैं :
(1) आगंतुक जीवाणुओं का भक्षण करती हैं,
(2) ये प्रतिपिंडों की रचना करती हैं,
(3) हिपेरिन उत्पन्न कर रुधिरवाहिकाओं में ये रुधिर को जमने से रोकती हैं,
(4) ये प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ कोशिका प्रोटीन की भी रचना करती हैं तथा
(5) हिस्टामिनरोधी कार्य कर शरीर को एलर्जी से बचाने में सहायक होती हैं।
रुधिर प्लेटलेट्स (Blood Platelets)
स्तनधारियों में रुधिर प्लेटलेट्स सूक्ष्म, रंगहीन, केन्द्रकविहीन गोलाकार तथा चक्रिक (discoidal) होती है। मेंढ़क के शरीर के रुधिर में छोटी-छोटी तर्क के आकार की केन्द्रक युक्त कोशिका थ्रोम्बोसाइट होती है। ये मेगाफेरियोसाइट कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य टुकड़े होते है, ये अनियमित आकृति की होती है | इनमें केंद्रक का अभाव होता है , इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है | इनका विनाश यकृत प्लीहा में होता है |
ये प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में 2.5 लाख से 5 लाख तक होते हें। इनका आकर 2.5 म्यू होता है। इनका जीवन चक्र चार दिन का होता है। इनके कार्य निम्नलिखित हैं :
(1) ये रुधिर के जमने (स्क्रंदन) में सहायक होते हैं तथा
(2) रुधिरवाहिका के किसी कारणवश टूट जाने पर ये टूटे स्थान पर एकत्र होकर कोशिकाओं को स्थिर करते हैं।

लसीका (Lymph)
यह अर्ध पारदर्शी क्षारीय तरल है, जो रुधिर कोशिकाओं तथा ऊतक के बीच स्थित होता है। इसमें RBCs अनुपस्थित तथा प्लाज्मा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसमें प्लाज्मा तथा ल्यूकोसाइट पाई जाती है। रुधिर की अपेक्षा इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम जबकि CO, एवं अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
लसीका के कार्य (Functions of Lymph)
- जल का अस्थायी संचय
- अधिशेष जल का अवशोषण
- दीर्घाणुओं का परिवहन, जैसे- प्रोटीन, हॉर्मोन आदि को रुधिर परिसंचरण में ले जाता है चूँकि ये अणु रुधिर कोशिकाओं की भित्तियों को नहीं भेद पाते । यही कारण है कि ये अणु सीधे रुधिर परिसंचरण में नहीं पहुँच पाते हैं।
- वसा का परिवहन
- संक्रमण से सुरक्षा – लिम्फोसाइट की मौजूदगी के कारण होता है ।
लसीका एवं रुधिर में अन्तर
| लसिका | रुधिर |
| लसीका में श्वेत रुधिर कणिकाएँ अधिक संख्या में होती हैं। | रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाएँ लसीका के अनुपात में कम संख्या में होती हैं। |
| लसीका में फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है, फिर भी थक्का जमने की शक्ति इसमें निहित होती है। | रुधिर में फाइबिनोजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह आसानी के साथ थक्का बन जाता है। |
| लसीका द्रव रंगहीन होता है। | रुधिर का रंग लाल होता है। |
| लसीका में लाल रुधिर कणिकाएँ कम संख्या में होती हैं। | रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएँ अधिक संख्या में होती हैं। |
रुधिर का थक्का बनना, या जमना (रुधिर का स्कन्दन) (Blood Coagution)
रुधिर का रुधिर वाहिकाओं से बाहर आते ही रुधिर के अवयव एक जैल समान संरचना में परिवर्तित हो जाते है , जिसे रक्त स्कंदन कहते है | यह एक सुरक्षात्मक प्रणाली है जो घाव में रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है तथा रुधिर क्षति को रोकती है | सरल शब्रुदों में रुधिर द्रव होता है, पर शरीर से बाहर निकलने पर वह कुछ मिनटों में जम जाता है, जिसे थक्का या रक्त स्कंदनकहते हैं। थक्का बनने के समय का निर्धारण कई विधियों से किया जा सकता है।

रुधिर का थक्का बनने की विधियाँ या प्रक्रिया
रुधिर के जमने में (1) प्रथ्रोम्बिन, (2) कैल्सियम परमाणु, (3) फाइब्रिनोजिन और (4) थ्रांबोप्लास्टिन की आवश्यकता होती है। पहले तीन पदार्थ रक्त में रहते हैं और चौथा प्लेटलेट के टूटने से निकलता है। इनके अतिरिक्त ऐंट्थ्राम्बिन और हिपेरिन भी रहते हैं। ताप के नीचा होने और कैल्सियम को निकाल लेने से तथा जल मिलाकर रुधिर के पतला कर देने से रुधिर का जमना रुक जाता है। मैग्नीशियम तथा सोडियम सल्फेट को मिलाने से तथा हिपेरिन, जोंकसत और डिकूमेरिन आदि रुधिर के जमने में बाधक होते हैं। रुधिर के शीघ्र जमने में ऊष्मा, थ्रांबीन, ऐड्रीनलीन, कैल्सियम क्लोराड तथा विटामिन के (k) से सहायता मिलती है।
जब किसी कटे हुए भाग से रुधिर बाहर निकलता है, तब यह जैली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इसे स्कन्दन कहते हैं। रुधिर के थक्का बनने की क्रिया एक जटिल क्रिया है। जब किसी स्थान से रुधिर बढ़ने लगता है और यह वायु के आता है, तो रुधिर में उपस्थित थ्रॉम्बोसाइट्स टूट जाती है तथा इससे एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ मुक्त होकर रुधिर के प्रोटीन से क्रिया करता है तथा प्रोथॉम्बोप्लास्टीन नामक पदार्थ में बदल जाता है। यह प्रोथॉम्बोप्लास्टीन रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रॉम्बोप्लस्टीन बनाती है। थॉम्बोप्लास्टीन, कैल्शियम आयन (Ca+) तथा ट्रिपटेज नामक एन्जाइस के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथॉम्बिन को सक्रिय थ्रॉम्बीन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देती है।
यह सक्रिय थ्रॉम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजेन पर क्रिया करता है और उसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। फॉइब्रिन बारीक एवं कोमल तन्तुओं का जाल होता है। यह जाल इतना बारीक एवं सूक्ष्म होता है कि इसमें रुधिर के कण, विशेषकर RBC, फँस जाते हैं और एक लाल ठोस पिण्ड-सा बन जाता है। इसे रुधिर थक्का कहते हैं। थक्का बहने वाले रुधिर को बन्द कर देता है। रुधिर स्कन्दन के बाद कुछ पीला-सा पदार्थ रह जाता है जिसे सीरम कहते हैं। सीरम का थक्का नहीं बन सकता क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता हैं। रुधिर में प्रायः एक प्रति स्कन्दन होता है जिसे हिपेरिन कहते हैं। यह प्रोथॉम्बिन के उत्प्ररेण को रोकता है। इसी कारण शरीर में बहते समय रुधिर नहीं जमता।
रुधिर के थक्का बनने के दौरान होने वाली महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया; थ्रॉम्बोप्लास्टिन + प्रोथॉम्बिन + कैल्शियम = थ्रॉम्बिन;
थ्रॉम्बिन + फाइब्रिनोज़न = फाइब्रिन; फाइब्रिन + रुधिर रुधिराणु = रुधिर का थक्का
रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा-सा ऑक्जेलेट (सोडियम अयदा पोटैशियम ऑक्जेलेट) मिलाया जाता है।

रुधिर समूह (Blood Groups)
रुधिर समूह के खोजकर्ता कार्ल लैण्डस्टीनर थे, जिन्होंने 1902 में इसकी खोज की थी। रुधिर को चार समूहों में बाँटा गया है (i) समूह-A (ii) समूह-B (iii) समूह- AB एवं (iv) समूह – O
रुधिर समूह-A (Blood Group A) – इसमें प्रतिजन – A तथा प्रतिरक्षी – b पाए जाते हैं।
रुधिर समूह-B (Blood Group-B) – इसमें प्रतिजन – B तथा प्रतिरक्षी – a पाए जाते हैं। रुघिर समूह – AB (Blood Group-AB) इसमें प्रतिरक्षी अनुपस्थित रहता है तथा एन्टीजन- AB रहता है। इस समूह के व्यक्ति किसी भी समूह का रुधिर प्राप्त कर सकता है। इसलिए, इसे सर्वग्राही रुधिर समूह (Universal Blood Recipient) कहते हैं।
रुधिर समूह-O (Blood Group-O) – इसके खोजकर्ता डी कास्टलो तथा स्टल थे। इसमें प्रतिरक्षी-ab उपस्थित रहता है। लेकिन प्रतिजन अनुपस्थित रहता है। इस समूह का व्यक्ति किसी भी समूह को रुधिर प्रदान कर सकता है। इसलिए, इसे सर्वदाता समूह (Universal Blood Donor) कहते हैं।
एक रुधिर वर्ग के व्यक्ति को उसी वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। दूसरे वर्ग का रक्त देने से उस व्यक्ति की लाल रुधिर कोशिकाएँ अवक्षिप्त हो सकती हैं। पर समान वर्ग का रक्त देने से अवक्षेपण नहीं होता। दूसरे वर्ग का रक्त देने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। दुर्घटना में कही कट जाने से, या शल्य कर्म में कभी कभी इतना रक्तस्राव होता है कि शरीर में रक्त की मात्रा बहुत कम हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसी दशा में रोगी के शरीर में रुधिर पहुँचाने से उसकी प्राणरक्षा संभव होती है। उस समय रुधिरपरीक्षा द्वारा रोगी का रुधिर वर्ग मालूम कर, उसी वर्ग के रुधिरवाले मनुष्य का रुधिर लेकर, रोगी को दिया किंतु ओ (O) वर्ग का रुधिर ऐसा होता है कि उसको अन्य वर्गों के व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं। इस कारण ओ (O) वर्ग के रुधिर वाले व्यक्ति सर्वदाता (Universal Donors) कहे जाते हैं। एबी (AB) वर्ग के रुधिरवाले व्यक्ति अन्य सब वर्गों का रुधिर ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ये व्यक्ति सर्वग्रहणकर्ता (Universal Receipients) कहे जाते हैं। रक्त में आर, एच (Rh) तत्व भी होता है, जिसकी परीक्षा भी आवश्यक है।
| रुधिर समूह | लाल रुधिर कणिका में प्रतिजन | प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी | रक्तदान की संभावना |
| A | A | b | A तथा AB वर्ग के रक्तदान कर सकता है। |
| B | B | a | B तथा AB वर्ग को रक्तदान कर सकता है। |
| AB | A तथा B | कोई नही | किसी भी वर्ग का रुधिर प्राप्त (सर्वग्राही) कर सकता है, परन्तु केवल AB वर्ग के व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकता है। |
| O | कोई नही | तथा | किसी भी वर्ग को रक्तदान (सर्वदाता) कर सकता है, परन्तु o से ही रुधिर प्राप्त कर सकता है। |
मानव में रुधिर आधान (Blood Transfusion in Human Being)
मनुष्य के रुधिर समूहों में सामान्यतया कोई भी रुधिर – अभिश्लेषण (agglutination) नहीं होता। इसका कारण यह है कि किसी भी रुधिर समूह में अनुरूप (corresponding) प्रतिरक्षी एवं प्रतिजन उपस्थित नहीं होते अर्थात् प्रतिजन A के साथ प्रतिरक्षी-a, एन्टीजन-B के साथ प्रतिरक्षी – b उपस्थित नहीं होते।
यदि किसी रुधिर समूह के रुधिर को किसी ऐसे रुधिर वर्ग के रुधिर में मिश्रित कर दिया जाए जिसमें अनुरूप प्रतिजन एंव प्रतिरक्षी उपस्थित हैं, तब रुधिर की लाल कोशिकाओं का अभिश्लेषण हो जाएगा।
उदाहरण, A रुधिर समूह के रुधिर का, B रुधिर समूह के रुधिर में मिश्रण कर दें, तो रुधिर कोशिकाओं का अभिश्लेषण हो जाएगा। इसमें लाल रुधिर कोशिकाएँ एक-दूसरे से चिपक जाती हैं।
इस प्रकार के चिपकाव के फलस्वरूप रुधिर वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है एवं प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अतः रुधिर आधान में एन्टीजन एवं प्रतिरक्षी का ऐसा ताल-मेल करना चाहिए, जिससे रुधिर का अभिश्लेषण न हो सके।
हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 2.5-17.5 ग्राम / 100 घन सेमी तथा स्त्रियों में 11.5-16.6 ग्राम / 100 घन सेमी होती है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है परन्तु लसीका में कम होती है। ब्लड बैंक में रुधिर 10°C पर सुरक्षित रहता है।
Rh कारक (Rh-factor)
1940 में लैण्डस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के प्रतिजन का पता लगाया। इन्होंने इस प्रतिजन की खोज रीसस नामक बन्दर में की थी। इसलिए, इस प्रतिजन का नामकरण Rh कारक (Rh-factor) किया गया।
जिन व्यक्तियों के रुधिर में यह तत्व पाया जाता है, उनका रुधिर Rh सहित (Rh+) कहलाता है तथा जिनके रुधिर में नहीं पाया जाता, उनका रुधिर Rh रहित (Rh–) कहलाता है। रुधिर आधान के समय Rh-कारक की भी जाँच की जाती है। Rh+ को Rh+ का रुधिर ही दिया जाता है। यदि Rh+ रुधिर वर्ग का रुधिर Rh– रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाए, तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु, जब दूसरी बार यदि इसी प्रकार रक्ताधान किया जाएगा तो रुधिर अभिश्लेषण के कारण Rh– रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।
यदि पिता का रुधिर Rh+ हो तथा माता का रुधिर Rh– हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरन्त बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम सन्तान के जन्म के समय होता है। इस बीमारी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस (Erythroblastosis Foetalis) कहते हैं।
विभिन्न समूह वाले माता-पिता से उत्पन्न होने वाले बच्चों के सम्भावित रुधिर समूह
| माता-पिता के रुधिर समूह | बच्चों में सम्भावित रुधिर समूह | बच्चों में असम्भावित रुधिर समूह |
| A x A | A या O | B या AB |
| A x B | O, A, B, AB | |
| A x AB | A, B, AB | O |
| A x O | O या A | B या AB |
| B x B | B या O | A, AB |
| B x AB | A, B, AB | O |
| B x O | O या B | A, AB |
| AB x AB | A, B, AB | O |
| AB x O | A, B | O, AB |
| O x O | O | A, B, AB |