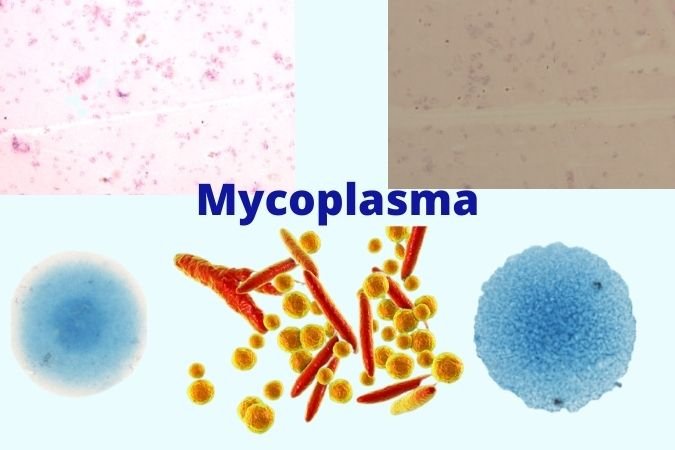What is Mycoplasma ?
माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम, एक कोशिकीय, बहुरूपी, प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इन्हें “पादप जगत का जोकर’ कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को विभिन्न तापमान, दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह ‘तापीय‘ या ‘अतापीय‘ प्लाज्मा हो सकता है।
माइकोप्लाज्मा की खोज नोकॉर्ड एवं रॉक्स 1898 ने की थी और इन्हें PPLO (Pleuro-Pneumonia Like Organism) कहा। माइकोप्लाज्मा अभी तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं ऑक्सीजन के बिना माइकोप्लाज्मा जीवित रह सकते हैं, और कई आकारों में पाए जाते है । उदाहरण के लिए, एम. जेनिटेलियम (M. Genitalium) फ्लास्क के आकार का (लगभग 300 x 600 nm) है, जबकि एम. न्यूमोनिया (M. Pneumoniae) अधिक लम्बा (लगभग 100 x 1000 nm) है। सैकड़ों माइकोप्लाज्मा की प्रजातियां जानवरों को संक्रमित करती हैं।
इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसलिए कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाली प्रतिजैविकों, जैसे पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं होता। और प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाहरी सीमा बनाती है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण ये जीव अपना आकार बदल सकते हैं

माइकोप्लाज्मा कोशिका की संरचना। जीवाणु यौन संचारित रोगों (sexually transmitted diseases), निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया और अन्य श्वसन विकारों (respiratory disorders) का प्रेरक एजेंट (causative agent)है। कई एंटीबायोटिक दवाओं से यह अप्रभावित होते है
माइकोप्लाज्मा का वर्गीकरण
- सन् 1966 में अंतरराष्ट्रीय जीवाणु नामकरण समिति ने माइकोप्लाज्मा को जीवाणुओं से अलग करके वर्ग- मॉलीक्यूट्स में रखा है।
- वर्ग- मॉलीक्यूट्स
- गण- माइकोप्लाज्माटेल्स
- वंश- माइकोप्लाज्मा
माइकोप्लाज्मा के लक्षण
आनुवंशिक सामग्री एक एकल डीएनए डुप्लेक्स है और नग्न है। (Genetic material is a single DNA duplex and is naked)
यह राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं।
इनमें DNA तथा RNA दोनों उपस्थित होते हैं।
एक कठोर कोशिका भित्ति (Rigid Cell Wall) की कमी के कारण, Mycoplasmataceae गोल से लेकर आयताकार आकार की एक विस्तृत श्रृंखला में विपरीत हो सकता है। इसलिए उन्हें छड़, कोक्सी (spherical) या स्पाइरोकेट्स (long) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
इन जीवों पर उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाले प्रतिजैविकों (जैसे – टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल) आदि का प्रभाव पड़ता है।
इनमें जनन द्विखण्डन, मुकुलन तथा एलिमेन्टरी बॉडीज द्वारा होता है।
ये किसी जीवित जंतु या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। तथा उनमे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कई बार ऐसे जीव मृत कार्बनिक पदार्थों पर मृतोपजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। यह परजीवी अथवा मृतोपजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
इनका आकार 100 से 500 nm तक होता है। इसलिए इन्हें जीवाणु फिल्टर से नहीं छाना जा सकता है।
इन्हें वृद्धि के लिए स्टेरॉल की आवश्यकता होती है।
माइकोप्लाज्मा प्रजातियां अक्सर research laboratories में कोशिका संवर्धन (cell culture) में contaminants के रूप में पाई जाती हैं। [Mycoplasmal cell culture contamination occurs due to contamination from individuals or contaminated cell culture medium ingredients]
कुछ माइकोप्लाज्मा का प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है l जन्म के समय कम वजन होना या समय से पहले जन्मे शिशु, माइकोप्लाज्मा संक्रमण के लिए, अतिसंवेदनशील होते हैं l
माइकोप्लाज्मा की उपस्थिति पहली बार 1960 के दशक में कैंसर के ऊतकों के नमूनों में दर्ज की गई थी। तब से, कई अध्ययनों ने माइकोप्लाज्मा और कैंसर के बीच संबंध को खोजने और साथ ही कैंसर के गठन में जीवाणु कैसे शामिल हो सकता है, को साबित करने की कोशिश की l

(A) माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया कोशिकाएं (Mycoplasma pneumoniae cells) (Gram Stain)
माइकोप्लाज्मा की सिग्नेट-रिंग के आकार (signet-ring-shaped) की कोशिका ग्राम – (negative), होती है, और कोशिका का आकार 0.2–0.3 माइक्रोन होता है और सामान्य रूप से 1.0 माइक्रोन से छोटा होता है। कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्रोटीन और लिपिड बाहरी कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं और कोशिकाएं स्पष्ट रूप से फुफ्फुसावरणीय (pleomorphic) होती हैं, जिसमें गोलाकार, रॉड जैसी, बार जैसी, और सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देने वाले फिलामेंटस आकारिकी होती है। typical cell एक सिग्नेट रिंग के आकार का होता है। कोशिकाएं ग्राम – (negative), हल्के बैंगनी रंग की होती हैं जिसमें गिमेसा दाग (Giemsa stain) होता है
(B) M. Pneumoniae (एम. न्यूमोनिया) signet ring cell (Giemsa stain) – एम. न्यूमोनिया कोशिका हल्के बैंगनी रंग की होती है जिसमें गिमेसा दाग (Giemsa stain) होता है।
(C) एम। निमोनिया आमलेट जैसी कॉलोनियां (M. pneumoniae omelet-like colonies)
(D) एम. निमोनिया की शहतूत के आकार की कॉलोनियां (Mulberry-shaped colonies of M. Pneumonia)
माइकोप्लाज्मा जनित पादप रोग और उनकी पहचान
माइकोप्लाज्मा पौधों में लगभग 40 रोग उत्पन्न करते हैं। जो निम्न लक्षणों द्वारा पहचाने जा सकते हैं।
पत्तियां पीली पड़ जाती हैं अथवा एंथोसाइएनिन वर्णक के कारण लाल रंग की हो जाती हैं।
पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है।
पुष्प पत्तियाँ आकार में बदल जाते हैं।
पर्व छोटी पड़ जाती है।
पत्तियाँ भुरभुरी हो जाती है।
माइकोप्लाज्मा जनित पादप रोग से प्रभावित पौधे
चंदन का स्पाइक रोग
आलू का कुर्चीसम रोग
कपास का हरीतिमागम
बैंगन का लघु पर्ण रोग
गन्ने का धारिया रोग
ऐस्टर येलो आदि
माइकोप्लाजमा जनित मानव रोग
अप्रारूपिक निमोनिया – माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी के कारण होता है।
माइकोप्लाज्मा जनित जंतु रोग
भेड़ और बकरियों का एगैलेक्टिया – माइकोप्लाज्मा एगैलेक्टी के कारण होता है।
माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग का उपचार
माइकोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न रोग का उपचार टेट्रोसाइक्लिन औषधि द्वारा किया जाता है